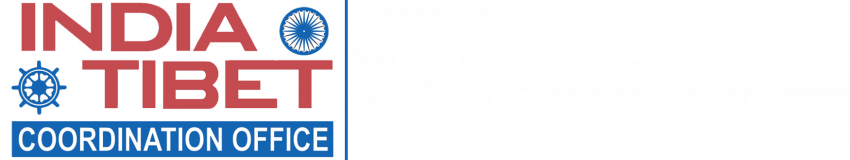नवभारत टाइम्स, 24 नवंबर 2014
 तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने अभी के हिंदुत्व को लेकर जो बात कही है, उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उनकी राय कोई उपदेश नहीं, एक शुभचिंतक पड़ोसी की सलाह है। पड़ोसी इस अर्थ में कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते वे हिंदुत्व को अच्छी तरह समझते हैं। दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन के मौके पर उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू धर्म में विचार-विमर्श के केंद्रों की बजाय मंदिरों की संख्या आखिर क्यों बढ़ती जा रही है?
तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने अभी के हिंदुत्व को लेकर जो बात कही है, उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उनकी राय कोई उपदेश नहीं, एक शुभचिंतक पड़ोसी की सलाह है। पड़ोसी इस अर्थ में कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते वे हिंदुत्व को अच्छी तरह समझते हैं। दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन के मौके पर उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदू धर्म में विचार-विमर्श के केंद्रों की बजाय मंदिरों की संख्या आखिर क्यों बढ़ती जा रही है?
उन्होंने कहा कि भारत ने कई बड़े विचारक दुनिया को दिए, लेकिन आज सारा जोर सिर्फ पूजा-पाठ और कर्मकांड पर है। असल में इस बात के जरिये दलाई लामा ने एक कड़वी सचाई की ओर इशारा किया है। यह बात सही है कि जब से देश में धर्म का राजनीतिकरण बढ़ा है, तब से यहां शांतिपूर्ण धार्मिक-आध्यात्मिक विमर्शों की जगह कम हुई है और पूजा स्थलों की संख्या अनाप-शनाप ढंग से बढ़ी है।
रोज नए-नए बाबा और धर्मोपदेशक सामने आ रहे हैं। साथ में उनके भ्रष्टाचार के किस्से भी सुनाई पड़ रहे हैं। धर्म की अगुआई में वर्षों से कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं दिखा, जिससे समाज में कोई सकारात्मक हलचल पैदा हुई हो। यंग जेनरेशन के लिए बस टीका लगाना और कलावा बांधना ही हिंदुत्व है। धर्म अब उन्हें कोई वैचारिक ऊर्जा नहीं देता। उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में विवेकानंद जैसे विचारक ने हिंदुत्व का एक वैचारिक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया था। वे तमाम रूढ़ियों, यहां तक कि मूर्ति पूजा को भी अनावश्यक मानते थे और समाज में व्यापक बदलाव को ही धर्म का आदर्श मानते थे। एक जगह उन्होंने लिखा है कि ‘कर्मयोगी के लिए जरूरी नहीं कि वह किसी सिद्धांत विशेष का अनुगमन करे या आत्मा आदि के सवालों पर विचार करे। भगवान में विश्वास करना भी कर्मयोगी के लिए अपरिहार्य नहीं है।’
 उनके अनुसार ‘जीवन का मूल प्रतिमान आस्तिकता नहीं, नैतिकता है, जिसका सार है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, शोषण को विशेषाधिकार मानने वाली व्यवस्था के विनाश के लिए संघर्ष।’ लेकिन उस विचार को हिंदू समाज ने छोड़ दिया। हिंदुत्व अब ऐसे यथास्थितिवादी लोगों के हाथ में है, जो धर्म को सिर्फ एक कारोबार मानते हैं। उन्होंने इसकी जनतांत्रिकता खत्म कर दी। वे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इससे उनका विशेषाधिकार खत्म हो सकता है। हिंदुत्व एक खास तरह की राजनीति में सिमटकर रह गया है। यह आयोजन भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की सरपरस्ती में किया गया है, जिनकी ‘हिंदू’ और ‘हिंदुत्व’ को लेकर राय जगजाहिर है। अगर इस सम्मेलन में खुली सोच वाले विद्वानों-विचारकों को बुलाया जाता तो इसका स्वरूप व्यापक हो सकता था। अब हिंदू समाज को तय करना है कि वह एक बंद राजनीतिक समुदाय बनकर संतुष्ट रहना चाहता है, या सबको साथ लेकर चलने वाले विश्वव्यापी जीवन मूल्य के रूप में हिंदुत्व की पुरानी पहचान को दोबारा हासिल करना चाहता है।
उनके अनुसार ‘जीवन का मूल प्रतिमान आस्तिकता नहीं, नैतिकता है, जिसका सार है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, शोषण को विशेषाधिकार मानने वाली व्यवस्था के विनाश के लिए संघर्ष।’ लेकिन उस विचार को हिंदू समाज ने छोड़ दिया। हिंदुत्व अब ऐसे यथास्थितिवादी लोगों के हाथ में है, जो धर्म को सिर्फ एक कारोबार मानते हैं। उन्होंने इसकी जनतांत्रिकता खत्म कर दी। वे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इससे उनका विशेषाधिकार खत्म हो सकता है। हिंदुत्व एक खास तरह की राजनीति में सिमटकर रह गया है। यह आयोजन भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की सरपरस्ती में किया गया है, जिनकी ‘हिंदू’ और ‘हिंदुत्व’ को लेकर राय जगजाहिर है। अगर इस सम्मेलन में खुली सोच वाले विद्वानों-विचारकों को बुलाया जाता तो इसका स्वरूप व्यापक हो सकता था। अब हिंदू समाज को तय करना है कि वह एक बंद राजनीतिक समुदाय बनकर संतुष्ट रहना चाहता है, या सबको साथ लेकर चलने वाले विश्वव्यापी जीवन मूल्य के रूप में हिंदुत्व की पुरानी पहचान को दोबारा हासिल करना चाहता है।